पत्थर पर घास की तरह उगते वैकल्पिक मीडिया का साल
वीडियो बनाने की आसानी, विचार की जटिलता और सरकार के खिलाफ साहस का संतुलन साध पाने वालों को अब पत्रकार नहीं सोशल इंफ्लुएंसर कहा जाता है.
यू ट्यूब पर खबर और राजनीति के लिए सबसे अधिक देखे जाने वाले शुरूआती 15 इंफ्लुएंसरों की लिस्ट देखने से अंदाजा हो जाता है कि औसतन उन्हें देखने वालो की संख्या अखबारों के फर्जी सर्कुलेशन से कहीं ज्यादा है. उनका मुकाबला तकनीक संपन्न सरकारी भोंपुओं से है और वे अपना मजबूत आधार या कांस्टिट्यूएंसी बनाने की ओर बढ़ चले हैं. प्रतिक्रिया में आई गालियों से पता चलता है कि उनका असर हो रहा है. यहां यह ध्यान देने की जरूरत है कि हिंदी अखबारों में एक पत्रलेखक रखा जाता था जो पाठकों की चुप्पी में बैठकर उनकी तरफ से काल्पनिक मीठे पत्र संपादक के नाम लिखा करता था.
इस लिस्ट में अजीत अंजुम का नाम है जो पहले तमाम एंकरों की ही तरह टेलीविजन में एक एंकर हुआ करते थे. किसान आंदोलन के दौरान अंजुम को लोगों ने अपनी पिछली तथाकथित निष्पक्ष संस्थानिक पत्रकारिता का प्रायश्चित करते देखा और उनका पुनर्जन्म हुआ. फिर देशभक्त के आकाश बनर्जी हैं जिनका व्यंग्य ओवरएक्टिंग के बावजूद निशाने पर लग रहा है. अभिसार शर्मा जो लाउड है लेकिन सफल हैं. पुण्य प्रसून बाजपेई जिन्हें हथेलियों के अतिघर्षण और उलझी भाषा के बीच आलोचना की ताकत संभाल लेती है.
ध्रुव राठी, साक्षी जोशी, श्याम मीरा सिंह और मीना कोटवाल समेत तमाम नाम हैं जो इस लिस्ट में ऊपर नीचे होते रहते हैं. यहां इन यू-ट्यूबरों की छवि और देहभाषा पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि विजुअल मीडिया में एंकर का मेकअप, पत्रकारिता में उसका पहला योगदान हुआ करता है. जो किसी खास छवि के लिए ही कराया जाता है.
इंफ्लुएंसरों की एक और लिस्ट है जिनकी औसत उम्र काफी कम है, विचार की जगह लोकप्रियतावाद है लेकिन इसी कारण पहुंच और प्रभाव इन पत्रकारों से बहुत ज्यादा है. इनमें अजेय नागर (कैरीमिनाटी), कामेडियन अमित भड़ाना, आशीष चंचलानी, भुवन बाम, गौरव चौधरी (टेक्निकल गुरूजी) के नाम लिए जा सकते हैं. इनकी लोकप्रियता के चलते फिल्म, आईपीएल और प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाने लगा है. युवाओं के बीच उनका दर्जा स्टार का है.
एक बात तो पक्की है कि चुनाव दर चुनाव देश में सोशल मीडिया और मोबाइल यूजरों की केमिस्ट्री का प्रभाव बढ़ता जा रहा है. असली खतरा यहां भी वही पुराना है क्योंकि तकनीक और पैसा किसी और के हाथ में है. कल को इस नए मीडिया के पत्रकारों का सामाजिक प्रभाव और दायरा बड़ा होगा तो उन्हें व्यापारिक कंपनियां मरोड़ कर अपने अनुकूल राजनीति का गुणगान करने के लिए के बाध्य कर सकती हैं. कितने पुराने कंचन के पीछे टूट कर जाएंगे और कितने नए लोकतंत्र की पहरेदारी के लिए आएंगे उनके बीच का अनुपात ही भविष्य तय करेगा.
 दिल्ली में भड़काऊ भाषण: नफरती नेता, पत्रकार और पुलिस का गठजोड़?
दिल्ली में भड़काऊ भाषण: नफरती नेता, पत्रकार और पुलिस का गठजोड़?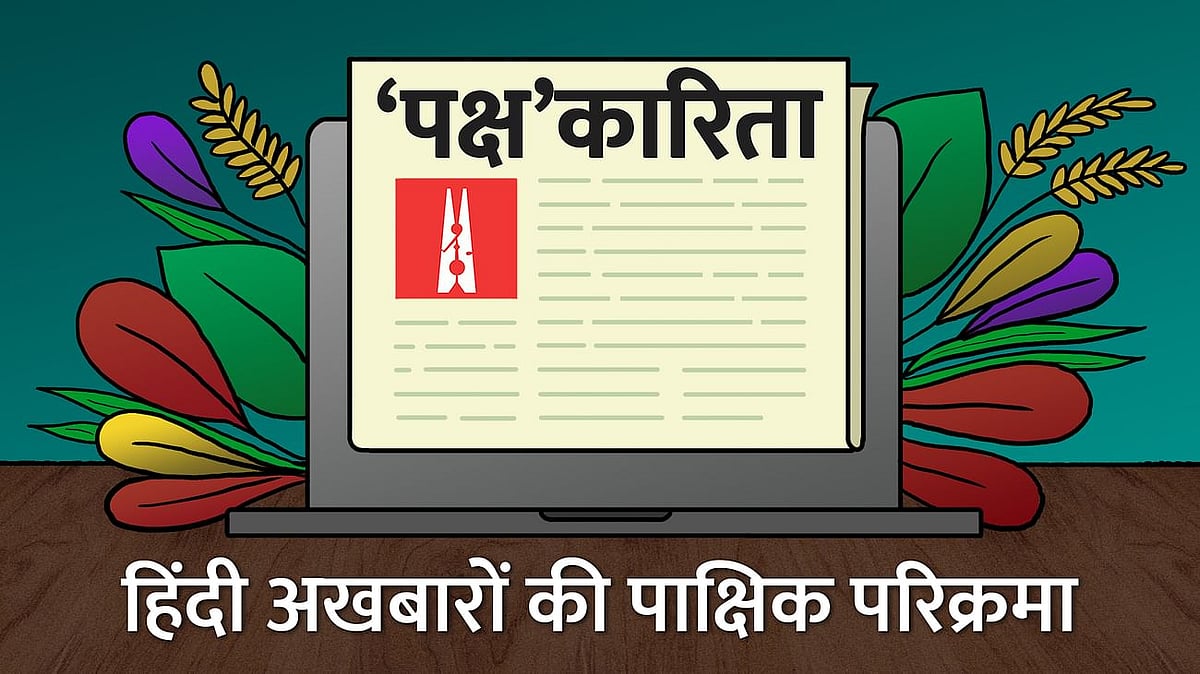 'पक्ष'कारिता: हिंदी के अखबार और संपादक हमेशा राम-रावण क्यों खेलते रहते हैं?
'पक्ष'कारिता: हिंदी के अखबार और संपादक हमेशा राम-रावण क्यों खेलते रहते हैं?