पंजाब में नोटा से भी कम वोट मिलने पर कम्युनिस्ट पार्टियों पर कोई चर्चा नहीं
उत्तर प्रदेश में बसपा के एक सीट जीतने पर बौद्धिक समाज में जैसी खलबली देखी गई वैसी कम्युनिस्ट पार्टी के बंगाल में लगातार दो बार हारने के बाद भी नहीं देखी गई.
यह समस्या से निकल भागने का एक तर्क तो हो सकता है, लेकिन समस्या से सीखने और हल निकालने वाली बात नहीं हो सकती. जैसे, इस बार के पंजाब विधानसभा चुनावों के ठीक पहले तक पंजाब के किसान और अन्य समुदाय के लोग दिल्ली की सीमाओं पर आकर डटे रहे. उनकी कुल मांग क्या थी? यदि इसे एक वाक्य में कहा जाय तो- खेती की लागत में कमी करो या लागत के अनुसार उत्पाद का दाम दो. वे खेत और खेती की सुरक्षा की मांग कर रहे थे. यदि इस सूत्र को थोड़ा और हल करें तो पंजाब के लोग आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की बेहतरी की मांग कर रहे थे. पंजाब में विधानसभा चुनाव के परिणाम इसके अनुरूप ही रहे. आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली के अनुभवों को पंजाब के लोगों के साथ जोड़ने में सफल रही, लेकिन यह भी सच है कि यह एक तात्कालिक हल ही है.
‘आप’ को चुनने से जुड़ी तात्कालिकता या भाजपा की उन्मादी राजनीति से चुनाव लड़ रही पार्टियों का पतन सीधे-सीधे जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं लगता है. यह समस्या चुनाव की राजनीति से जुड़ी हुई है. किसी विचारधारा का चुनाव में उतरने का अर्थ चुनावी राजनीति के दांवपेंच में अपने कार्यक्रम को उतारना होता है, इसकी सीमाओं और संभावनाओं को देखना होता है. यदि लगता है कि चुनाव उसके कार्यक्रम और विचारधारा को बुरी तरह प्रभावित कर जाएंगे तब उसे अपने निर्णयों से पीछे हटना होता है और जनता की गोलबंदी पर नयी रणनीति और कार्यनीति को तलाशना होता है. मुझे लगता है कि सीखने का अर्थ यही होता है. सीपीआई और सीपीएम को देखकर लगता है कि वे सीखने से अभी दूर हैं. बंगाल के चुनाव की समीक्षाएं फिलहाल यही बताती हैं. पंजाब के चुनाव से उन्होंने क्या सीखा, अभी देखना बाकी है.
बौद्धिक समुदाय में जितनी बेचैनी इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा को एक सीट आने को लेकर दिखी उतनी बंगाल में लगातार दो बार सीपीएम के पतन में नहीं दिखी और न ही यह पंजाब में कुल वोटों की गिनती में कम्युनिस्ट पार्टियों के नोटा से भी पिछड़ जाने में दिखी. क्या यह सामाजिक न्याय की अवधारणा में वोटों के विभाजन और ध्रुवीकरण के गणित में आ रही गड़बडियों की वजह से हुआ है? या यह मान लिया गया है वोटों के ध्रुवीकरण का पैटर्न जाति आधारित ही हो सकता है और इसे ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी बनाकर ही प्रभावित किया जा सकता है? क्या सामाजिक अवधारणा में वर्ग लुप्त होती प्रजाति बन गई है?
कई बार राजनीतिक विश्लेषण आर्थिक कारकों से इतनी दूर चले जाते हैं कि उनके निष्कर्ष महज सच का आभास देते हैं, लेकिन सच से काफी दूर होते हैं. हारी हुई पार्टियां भी ऐसे निष्कर्ष पर भरोसा करने लगती हैं क्योंकि इससे वे कई कठिन सवालों से बच निकलती हैं जिनका सामना किए बिना सच तक पहुंचना मुश्किल है. एक समय था जब उत्तर प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टियों ने हार का ठीकरा जातिवादी राजनीति के सिर पर दे मारा था. आज यही काम वे धार्मिक उन्माद के सिर पर अपनी हार का दोष मढ़कर कर रही हैं.
चुनाव राज्य द्वारा संचालित निहायत ही नियंत्रित प्रक्रिया होती है और वह इसे अपने चरित्र के अनुरूप ही संपादित करता है. फिर भी इसमें विचलन होते हैं और इसे विश्लेषणों में परखा जा सकता है. चुनाव न तो सामाजिक न्याय करते हैं और न ही समाज का मौलिक रूपांतरण, लेकिन इसके परिणामों में छुपे हुए इस तरह के चिह्नों को देखा जा सकता है. चुनाव मूलतः प्रतिनिधित्व की एक प्रक्रिया होती है. यह तभी संभव होता है जब प्रतिनिधि की विविधता की जद्दोजहद समाज के भीतर भी मौजूद हो. ऐसा न होने पर राजनीतिक विश्लेषकों की भूमिका और भी बढ़ जाती है.
मुझे उम्मीद है कि चुनाव के विश्लेषण के तौर-तरीके बदलेंगे और उन तकनीकों का प्रयोग होना शुरू होगा जहां से धर्म या जाति या दोनों का ही विश्लेषण संभव होगा तथा सामाजिक चिन्तन की प्रक्रिया को समझना संभव होगा.
(साभार- जनपथ)
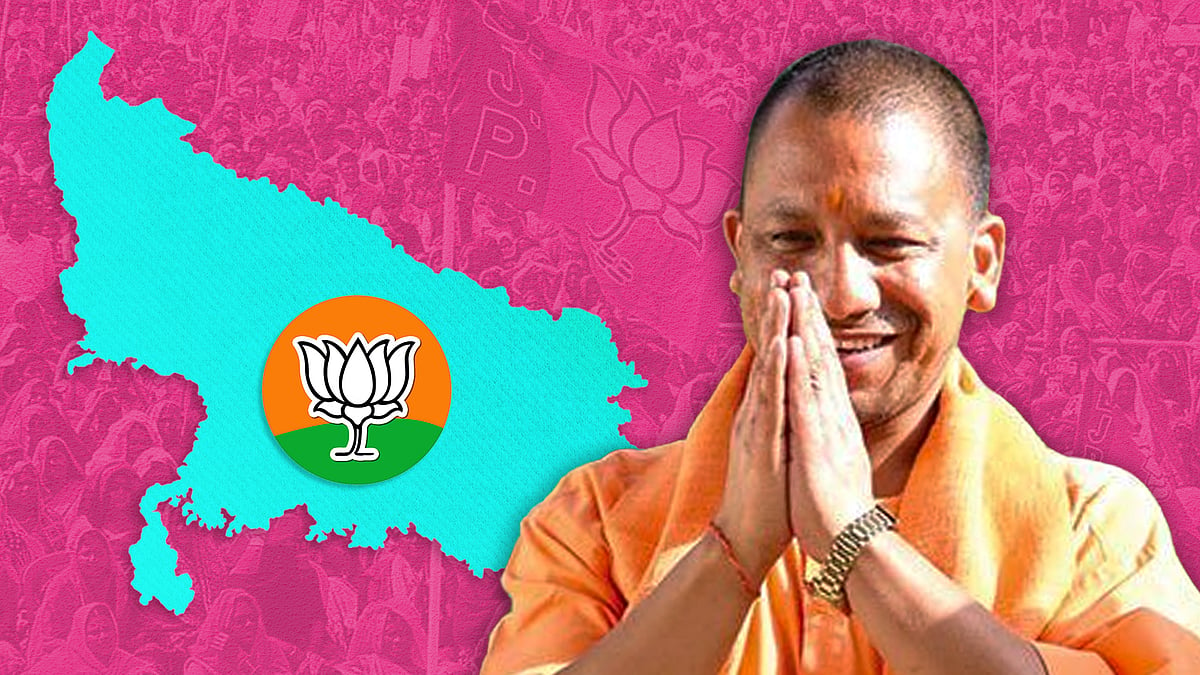 चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की किस्मत का रोड़ा कहां अटका?
चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की किस्मत का रोड़ा कहां अटका? पंजाब चुनाव के वो चेहरे जिन्होंने दिग्गज नेताओं को दी शिकस्त
पंजाब चुनाव के वो चेहरे जिन्होंने दिग्गज नेताओं को दी शिकस्त