'पक्ष'कारिता: हिंदी के अखबार हिंदी के लेखकों को क्यों नहीं छापते हैं?
आप जागरण पढ़ें, जनसत्ता पढ़ें या हिंदुस्तान, केवल दुकान अलग-अलग है लेकिन माल एक.
एक और दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिला. आजकल नौकरशाहों और बड़े ओहदेदार अधिकारियों के नाम से प्रचारात्मक लेख लिखे जा रहे हैं और थोक के भाव छोटे अखबारों को फ्री में बांटे जा रहे हैं. मसलन, गांधीनगर में रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण हुआ. उसकी सराहना करते हुए भक्ति में शराबोर एक लेख छपा कुछ छोटे अखबारों में एक ही दिन. सब एडिट पेज पर प्रमुख तरीके से. लिखने वाले हैं भारतीय रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी और सीईओ एसके लोहिया. यह लेख 16 जुलाई को स्वदेश, आजाद सिपाही सहित ढेर सारे अखबारों में छपा है. बिलकुल इसी तरह सिक्योरिटी कंपनी चलाने वाले भाजपा सांसद आरके सिन्हा के नाम से एक लेख कई जगह छपा है उसी दिन, जिसमें वे बिहार में खेलों की स्थिति पर चिंता जता रहे हैं.

बीते पखवाड़े देश के सबसे बड़े अखबार दैनिक भास्कर पर छापा पड़ा, उस छापे की राख से अखबार स्वतंत्र वीर बनकर निकला लेकिन इस खबर के पीछे की समूची वैचारिकी को तमाम हिंदी के अखबार गड़प कर गए. कम से कम बिरादरी का साथ निभाने के नाम पर अभिव्यक्ति की आजादी के हक में एक लेख तो बनता था, लेकिन किसी ने नहीं छापा. संपादकीय तो दूर की बात रही. यहां फिर मैदान खाली छूटा तो जागरण ने बलबीर पुंज का लेख 29 जुलाई को छाप दिया जिसमें हाइलाइट किये हुए शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, तो एजेंडा समझ में आ जाएगा. किसानों पर भी अब कहीं लेख नहीं छप रहे हैं, लेकिन अकेले जागरण है जो बदनाम करने से अब भी बाज़ नहीं आ रहा है. उसके संपादकीय पन्ने पर एक कॉलम में कहीं-कहीं के ब्यूरो प्रमुखों की टिप्पणी छपती रहती है. उसी में हरियाणा और पंजाब के ब्यूरो चीफ लगातार किसान-विरोधी एजेंडा ताने हुए हैं.
आवाज़ आ रही है क्या?
वास्तव में, मूल हिंदी में वैचारिक लेखों को ज्यादा जगह देने के कारण दैनिक जागरण से ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जो छूट गया हो. हर एक प्रासंगिक और बहसतलब मुद्दे को उसने राष्ट्रवादी मुहावरे में सरकारी पक्ष के साथ बड़े विस्तार से सजाकर प्रस्तुत किया. हिंदी के सारे अखबार मिलकर भी इतना नहीं कर पाए. चूंकि यह अध्ययन 15 दिनों का ही है तो माना जा सकता है कि मोटे तौर पर ट्रेंड यही रहता होगा क्योंकि संपादकीय पन्ना एक स्थायी किस्म की संरचना है जिसमें ज्यादा फेरबदल नहीं किया जाता है. एक अहम बात यह समझ में आती है कि अचानक आए पेगासस जैसे विशिष्ट मुद्दों को छोड़ दें, तो कोरोना की वैक्सीन से लेकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति-रणनीति, जनसंख्या, सरकारी योजनाएं, ओलिंपिक, संसद, किसान आदि पर सभी अखबारों का सुर एक सा है. इस लिहाज से कह सकते हैं कि संपादकीय विचार के लिहाज से दैनिक जागरण के इर्द-गिर्द बाकी तमाम हिंदी अखबार उपग्रहों की तरह घूमते नजर आते हैं.
यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जब पेगासस और दैनिक भास्कर के छापे पर कुछ ट्वीट करने की जरूरत महसूस होती है तो उन्हें हिंदी अखबार की कोई कतरन इस विषय पर नहीं मिलती. फिर वे बुंदेलखंड वाली जिज्जी का वीडियो ट्वीट कर देते हैं और इस तरह राजनीतिक कर्तव्य निभा लेते हैं. सोचिए, ये हाल हो गया है अखबारों का. उधर दूसरी ओर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ट्वीट करने के लिए अखबारों की बाढ़ लगी हुई है जो उन्हें अगले साल चुनाव जितवाने की भविष्यवाणी और सर्वे छाप रहे हैं.
दिल्ली में जब इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में लॉन्च हुआ था, तो उसमें संपादकीय पन्ना छपता था. उसी दिन के अंग्रेजी लेखों का अनुवाद कर के लगाना होता था. दो महीने की कवायद में संपादक को ज्ञान हो गया कि सारी मेहनत व्यर्थ है, ये सब कोई नहीं पढ़ता. इसलिए संपादकीय पन्ना ''स्टार्ट-अप'' पन्ने में बदल दिया गया. हिंदी में वैचारिक लेखों की व्यर्थता का बोध सबसे पहले दैनिक भास्कर को श्रवण गर्ग के संपादकत्व के आखिरी वर्षों में हुआ जब भोपाल मुख्यालय ने विज्ञापन के चक्कर में संपादकीय पन्ने को ही गिराना चालू कर दिया. यह अभूतपूर्व था, लेकिन ट्रेंडसेटर बनने की ताकत रखता था. आज थोड़ा लाज-लिहाज में भले अखबार संपादकीय पन्ने को बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन वास्तव में उसके होने और न होने के बीच बहुत फर्क नहीं है. कर्पूरचंद्र कुलिश की परंपरा वाली पत्रकारिता में अगर आपको संपादकीय पन्ने पर लीड लेख के रूप में गुलाब कोठारी के धार्मिक प्रवचन पढ़ने पड़ें, तो पन्ने का नाम उस दिन बदल के धर्म-कर्म क्यों नहीं कर दिया जाता?
प्रेमचंद आज जीवित होते तो न अपनी पत्रिका चालू कर पाते न ही उन्हें कोई संपादकीय पन्ने पर छापता. फिर वे तमाम कामनाओं से मुक्त होकर क्यों लिखते और किसके लिए? हिंदी अखबारों के लिए आउटडेटेड हो चुके हिंदी के तमाम लेखकों, पत्रकारों और बौद्धिकों की तरह क्या वे भी फेसबुक पोस्ट लिख रहे होते? क्या वे भी घर में बैठ कर फेसबुक लाइव करते और दस बार पूछते- मेरी आवाज़ आ रही है क्या?
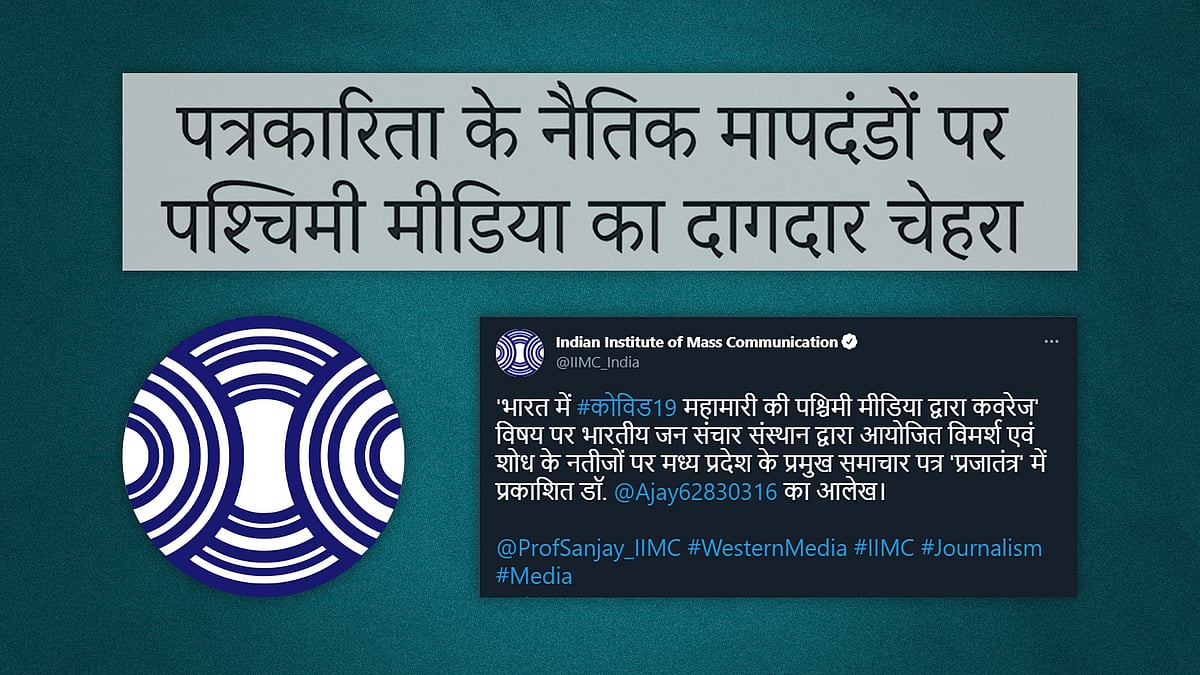 पश्चिमी मीडिया पर आईआईएमसी में सेमिनार और सर्वे: मीठा-मीठा गप्प, कड़वा-कड़वा थू
पश्चिमी मीडिया पर आईआईएमसी में सेमिनार और सर्वे: मीठा-मीठा गप्प, कड़वा-कड़वा थू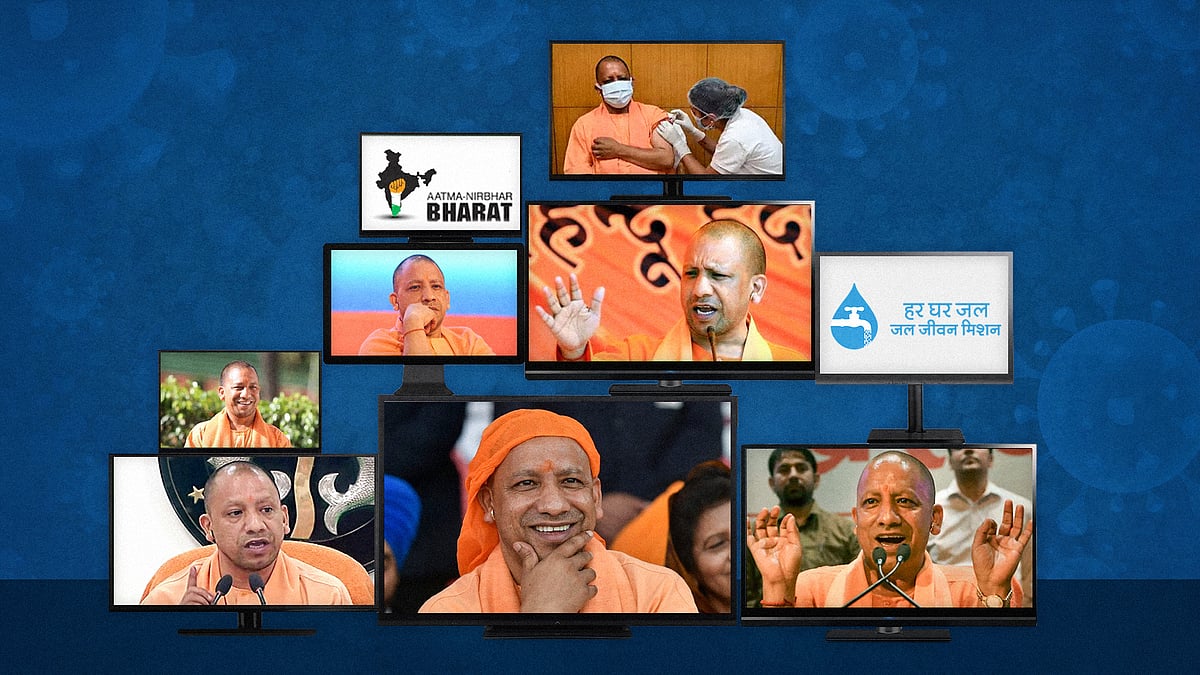 अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच योगी सरकार ने टीवी चैनलों को दिया 160 करोड़ का विज्ञापन
अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच योगी सरकार ने टीवी चैनलों को दिया 160 करोड़ का विज्ञापन


