16 साल पहले इरफान द्वारा लिखा गया एक लेख
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की त्रैमसिक पत्रिका ‘रंग प्रसंग’ के लिए इरफान खान ने रंगमंच और सिनेमा के संबंध पर यह लेख लिखा था. 16 साल पहले लिखे इस लेख में इरफान ने अपने अनुभवों से इस संबंध की पड़ताल के साथ अपनी राय रखी थी. उनकी याद में यह लेख...
रंगमंच और सिनेमा दोनों माध्यमों की पृथकता स्पष्ट है. आप रंगमंच में उस तरह से बातें नहीं कर सकते, जिस तरह से सिनेमा में करते हैं. रंगमंच में आपको हर चीज मंच पर दिखानी होती है. सिनेमा की परेशानी अलग है. वहां एक्टर को कम समय मिलता है. लाइटिंग और सेट की व्यवस्था में समय लगने पर निर्देशक परेशान नहीं होता, लेकिन अभिनेता दो-चार टेक ले ले या रिहर्सल की मांग करें तो निर्देशक खीझने लगता है. सिनेमा की एक्टिंग में आमतौर पर मेलोड्रामा की मांग रहती है. कुछ कर दिखाने की मंशा काम करती है. सूक्ष्मता से अधिक स्थूलता पर फोकस रहता है, जबकि होना उल्टा चाहिए.
सिनेमा में रंगमंच से आए अभिनेताओं पर थिएट्रिकल होने का अभियोग लगता रहा है. मुझे लगता है कि इस टर्म का उपयोग लापरवाही के साथ हो रहा है. हमारे समीक्षक प्रशिक्षित नहीं हैं. वे किसी भी पारिभाषिक शब्द को उसके अर्थ और संदर्भ से अलग ले जाकर इस्तेमाल करते हैं. आप रिव्यू पढ़ें तो यही मिलेगा कि उसने खुद को दोहराया, रोल के साथ न्याय किया, रोल निभा नहीं पाया. क्या एक्टिंग को ऐसे ही समझा और समझाया जाता है?
मुझे नहीं लगता कि रंगमंच से सिनेमा में आए अभिनेता को कोई खास महत्व दिया जाता है. कई बार अभिनेताओं का संघर्ष लंबा हो जाता है. हां, किसी प्रकार आपने जगह बना ली तो अवश्य रंगमंच से आने का उल्लेख किया जाता है. आपकी प्रतिभा का श्रेय रंगमंच को दे दिया जाता है. इसमें कोई बुराई नहीं है, पर कलाकार के वैयक्तिक प्रतिभा को भी तो रेखांकित करना चाहिए.
मैं अपनी बात कहूं तो आरंभ में कैमरे के आगे बहुत बंधा महसूस करता था. मुझे ज्यादा जूझना पड़ा. लगातार अभ्यास के बाद में कैमरे के आगे सहज हो सका. रंगमंच की आरंभिक ट्रेनिंग में जितना सीखा, उससे आगे कोई एडवांस ट्रेनिंग नहीं हुई. रंगमंच का प्रशिक्षण कई बार आड़े भी आता है. फिल्म देखते समय पता चलता है कि परफॉर्मेंस में झटका लग रहा है. समीक्षक भी उस पर गौर नहीं कर पाते. आम दर्शक की तो बात छोड़ें. खुद को एहसास होता है अपनी गलतियों का.
रंगमंच से आए कलाकारों में केवल राज बब्बर ने स्टारडम का सुख भोगा. वास्तव में स्टारडम खास व्यक्तित्व से मिलता है. रंगमंच से आए अभिनेता वैसा व्यक्तित्व नहीं गढ़ पाते. अमिताभ बच्चन की एक्टिंग में दोनों खूबियां झलकती है. अपने देश में अभिनय की तकनीक और बारीकी की जरूरत ही नहीं पड़ती. यहां तो मेलोड्रामा चलता है. रियल और स्वाभाविक एक्टिंग के दर्शन हॉलीवुड की फिल्मों में होते हैं. शायद हमारे दर्शक भी अभी वैसी एक्टिंग के लिए तैयार नहीं हैं. मुझे लगता है कि सिनेमा की एक्टिंग में अभी बहुत विकास होना है. सिर्फ व्यक्तित्व का खेल या स्टारडम का प्रभाव लंबे समय तक नहीं चलेगा.
संतुष्टि तो नहीं मिलती. सिनेमा की सीमित एक्टिंग में संतुष्टि नहीं है. इसके संतोष दूसरे प्रकार के हैं. भौतिक सुख और संतोष मिल जाता है. आपको लोग पहचानने लगते हैं. आपके पास सुविधाएं रहती हैं, लेकिन सृजनात्मक सुख गायब हो जाता है. फिल्मों की एक्टिंग करते समय खटकता रहता है कि जो लोगों को अच्छा लग रहा है या जिसकी तारीफ हो रही है वह उपयुक्त नहीं है. शायद इसी कारण में कई बार अधिक आनंद नहीं उठा पाता. वह विराग चेहरे पर भी आता होगा और सुधि दर्शकों को लगता है कि मैं ठहर गया हूं... जड़ हो रहा हूं. मैं इस जड़ता को तोड़ना चाहता हूं. कोशिश है कि काम करते समय मुझे अपने आप में लगे कि मैं सच्चा हूं.
अप्रैल-जून 2005
(यह लेख वरिष्ठ पत्रकार अजय ब्रह्मात्मज के विशेष सहयोग से प्रकाशित)
 फिल्म लॉन्ड्री: हिंदी फिल्मों में दलित चरित्र
फिल्म लॉन्ड्री: हिंदी फिल्मों में दलित चरित्र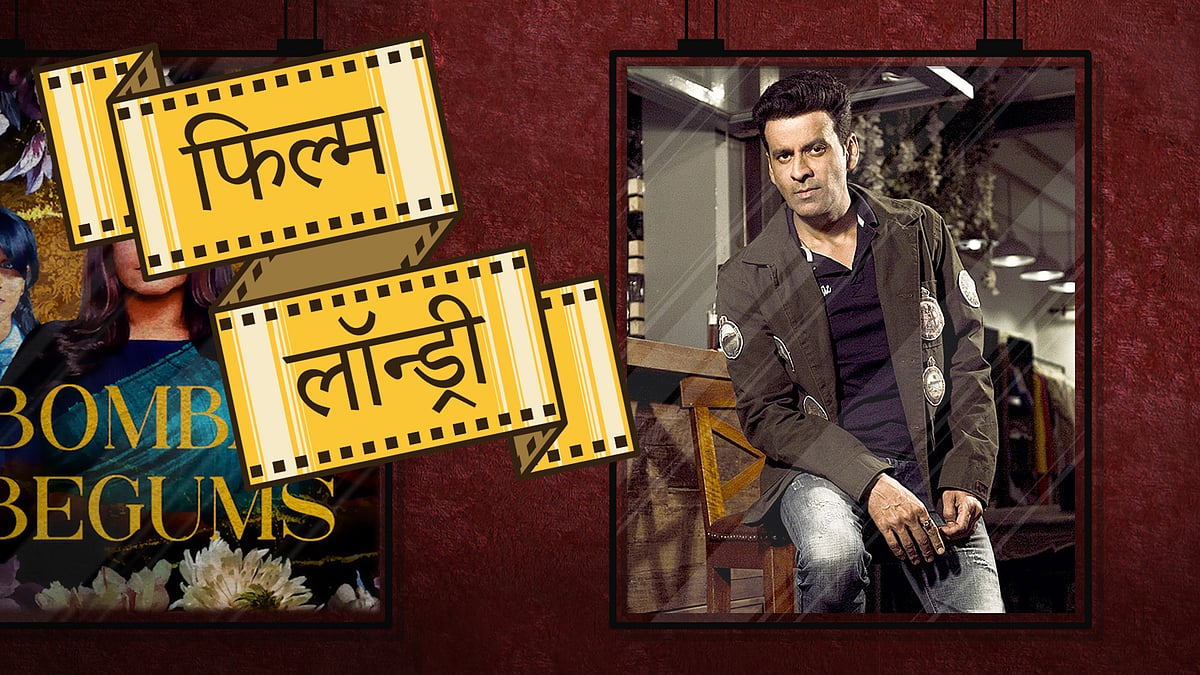 फिल्म लॉन्ड्री: "अभिनय के प्रति मेरा अथाह प्रेम ही मुझे अहन तक ले आया है"
फिल्म लॉन्ड्री: "अभिनय के प्रति मेरा अथाह प्रेम ही मुझे अहन तक ले आया है"