2024 का परिणाम: भारतीय राजनीति में आकार ले रहे तीन मूलभूत प्रश्न
इस नतीजे के बाद देश में विपक्ष और अधिक प्रासंगिक होगा, और अधिक ताकतवर होगा.
लोकसभा चुनाव के नतीजों को दो तरह से देखा जा सकता है. एक दलील यह हो सकती है कि इन परिणामों से अगली सरकार का चेहरा तय होगा. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगियों के साथ सरकार बनाएगी, इसमें कोई रुकावट नहीं दिखती है. यह सही मायनों में एक गठबंधन सरकार होगी और इस बात की संभावना न के बराबर है कि भाजपा या मोदी अपने सहयोगी दलों पर उस तरह का एकाधिकार जमा पाएंगे जैसा पिछले दस सालों में दिखा है.
दूसरी ओर, इंडिया गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन है. इस नतीजे के बाद देश में विपक्ष और अधिक प्रासंगिक होगा, और अधिक ताकतवर होगा. इस बात की प्रबल संभावना है कि विपक्ष की इस सफलता के बाद वो बहुत से पेशेवर राजनीतिक चेहरे, जो भाजपा के पाले में चले गए हैं, वो एक बार फिर से लौटें और कांग्रेस के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं.
लेकिन, आंकड़ों के खेल से अलग इस चुनावी नतीजे का एक और भी गंभीर पहलू है. ये नतीजा भारतीय राजनीति के तीन मूलभूत पहलुओं को फिर से परिभाषित करते हैं: भविष्य में भारत की सत्ता की प्रकृति कैसी होगी, नया राजनैतिक नैरेटिव क्या होगा और क्या अंततः सामाजिक मुद्दे एक बार फिर राजनीति के केंद्र में होंगे. इन पहलुओं की रोशनी में हमें 2024 के फैसले का निहितार्थ समझने की आवश्यकता है.
सबसे पहले राज्य की अपेक्षित भूमिका की बात कर लेते हैं. भाजपा का संकल्प पत्र (जिसे आधिकारिक तौर पर मोदी की गारंटी के रूप में जारी किया गया था) शासन के उस मॉडल के इर्द-गिर्द घूमता है जिसे मोदी सरकार ने पिछले दस वर्षों में बनाया और पोषित किया है. मैं इसे चैरिटेबल स्टेट कहता हूं-- यानि ऐसी सरकार जो उदार दिखने के लिए कल्याणकारी सामाजिक नीतियां बनाए, और दूसरी ओर खुलेआम एक बाजार समर्थक अर्थव्यवस्था के प्रति पूरी तरह से समर्पित भी रहे.
भाजपा ने इसी के मुताबिक अपनी चुनावी रणनीति तैयार की थी. यह रणनीति दो तर्कों पर आधारित थी जिसका जिक्र बार-बार किया गया. एक तर्क यह दिया गया कि कल्याणकारी योजनाएं नागरिकों को सशक्त बनाएंगी, इसकी मदद से वो खुले बाजार में सक्रिय रूप से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे. इस तरह चैरिटेबल स्टेट 'आर्थिक असमानता' के विवादित मुद्दे से निपट पाने में सफल रहेगा. दूसरा तर्क था कि सामाजिक योजनाओं का कार्यान्वयन धर्मनिरपेक्ष रूप से किया जाता है. प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार दोहराया कि उनकी कल्याणकारी नीतियां सब पर समान रूप से लागू होती हैं, इसमें किसी तरह का भेदभाव नही होता.
लेकिन कांग्रेस ने इस पक्ष में एक गंभीर चुनौती पेश की. उन्होंने नई आर्थिक नीति का प्रस्ताव रखा, जिसमें तीन लक्ष्य रेखांकित किए गए- रोजगार, पैसा, लोक कल्याण. इस नीति का तर्क है कि नागरिकों को सम्मानजनक रोजगार दिया जाय और सामाजिक कल्याण के लिए आर्थिक क्षेत्र को और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाया जाय. कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सरकार और पूंजीपतियों की साठगांठ और बढ़ते एकाधिकार के ऊपर अक्सर तीखे और दिलचस्प हमले भी किए. चुनाव प्रचार ने इस बहस को और तेज़ कर दिया. परिणामस्वरूप, यह सवाल विवाद का सबसे जरूरी विषय बन गया कि आर्थिक क्षेत्र में सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए. निकट भविष्य में राजनीतिक वर्ग इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकता.
राहुल गांधी की दो भारत जोड़ो यात्राएं इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक हैं.
इस चुनाव नतीजे का दूसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि इससे एक नया राजनीतिक कथानक उभरेगा. हिंदुत्व से प्रेरित राष्ट्रवाद पिछले एक दशक से भारतीय राजनीति पर हावी रहा है. भाजपा के साथ-साथ गैर-भाजपा दलों ने भी एक हद तक अपनी राजनीतिक रणनीति को इस कथानक से तालमेल बिठाते हुए स्वीकार कर लिया है. लेकिन इस बार कुछ रोचक हुआ. विपक्ष ने हिंदुत्व या राष्ट्रवाद पर कोई सीधी टिप्पणी किए बिना न्याय का विचार उठाया.
यह नया नैरेटिव 1990 के दशक की पुरानी सामाजिक न्याय की राजनीति का ही विस्तार है. इसमें आर्थिक असमानता और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ लेने के मुद्दे समाहित हैं. इस नए नैरेटिव ने भाजपा को वाकई बहुत असहज कर दिया है. यही कारण है कि भाजपा के नेतृत्व ने अंततः इस नैरेटिव को सांप्रदायिकता के हथियार से काटना चाहा. यह कहना कि कांग्रेस हिंदू ओबीसी/एससी से आरक्षण छीन लेगी और मुसलमानों को दे देगी, इसी राजनीतिक बेचैनी से उपजा है. गौरतलब है कि गैर-भाजपा दलों ने इस तरह के आरोपों पर सिर्फ इसलिए खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दी, कहीं उन्हें मुस्लिम समर्थक पार्टियों के रूप में न पेश कर दिया जाय. फिर भी, 'न्याय' ने एक उभरते राजनैतिक नैरेटिव के रूप में आकार लेना शुरू कर दिया है. चुनाव परिणाम इस तथ्य को साफगोई से रेखांकित करते हैं.
अब हम इस चुनाव के तीसरे नतीजे पर आते हैं, यानि सामाजिक मुद्दों को राजनीति के केंद्र में फिर से लाना. हमें याद रखना चाहिए कि भारत में चुनाव केवल आक्रामक अभियानों या चुनाव प्रचार के अन्य पेशेवर तरीकों पर निर्भर नहीं होते हैं. राजनीति सदैव सामाजिक स्तर पर आकार लेती है. पिछले कुछ सालों में भाजपा की सफलता, सामाजिक क्षेत्र में पार्टी की सक्रिय उपस्थिति का परिणाम है. आरएसएस और अन्य हिंदुवादी संगठनों की समाज के बीच सक्रिय गतिविधियों से भाजपा के लिए एक मजबूत आधार तैयार होता है. पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर राजनैतिक संवाद को बढ़ावा देना आसान हो जाता है. गैर-भाजपा दलों को अब तक यह लाभ नहीं मिला है.
राहुल गांधी की दो भारत जोड़ो यात्राएं इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक हैं. सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, जमीनी स्तर के आंदोलनों के नेताओं और सिविल सोसाइटी संगठनों ने इस पहल को तार्किक समर्थन दिया. इस बदलाव ने बहुत से लोगों को कांग्रेस का समर्थन करने का एक मजबूत नैतिक तर्क दिया. लोगों ने स्वीकार किया कि राहुल गांधी की यात्राओं का समर्थन किया जाना चाहिए ताकि राजनीतिक दल (इस मामले में कांग्रेस) और जमीनी स्तर पर लोगों के बीच एक संबंध स्थापित किया जा सके.
लेकिन साथ ही, सिविल सोसाइटी समूहों ने कांग्रेस से सैद्धांतिक दूरी भी बनाए रखी. इसका परिणाम स्पष्ट था. दोनों यात्राएं देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले सबसे वंचित समुदायों और अन्य समूहों को जागरूक करने में सफल रहीं. इन दो यात्राओं के दौरान लोगों ने जो मुद्दे उठाए और चर्चाएं की, उन्हें कांग्रेस के घोषणापत्र में शामिल किया गया. स्थानीय स्तर पर बनाई गई इन योजनाओं से यह राजनैतिक विमर्श समाज के निचले स्तर तक पहुंचा. जाहिर है, इसने हिंदुत्व के असर को पूरी तरह समाप्त नहीं किया; फिर भी इसने सामाजिक क्षेत्र को बहस और चर्चा का जीवंतता प्रदान की. खासकर उत्तर के राज्यों में. इस चुनाव के नतीजों के बाद इस प्रक्रिया को और बढ़ावा मिलेगा.
इस अर्थ में, 2024 का यह नतीजा हमें समझने में मदद करता है कि वर्तमान में हमारा लोकतंत्र किस दौर से गुजर रहा है.
 बनारसिया मिज़ाज, समाज और राजनीति पर व्योमेश शुक्ल से बातचीत
बनारसिया मिज़ाज, समाज और राजनीति पर व्योमेश शुक्ल से बातचीत 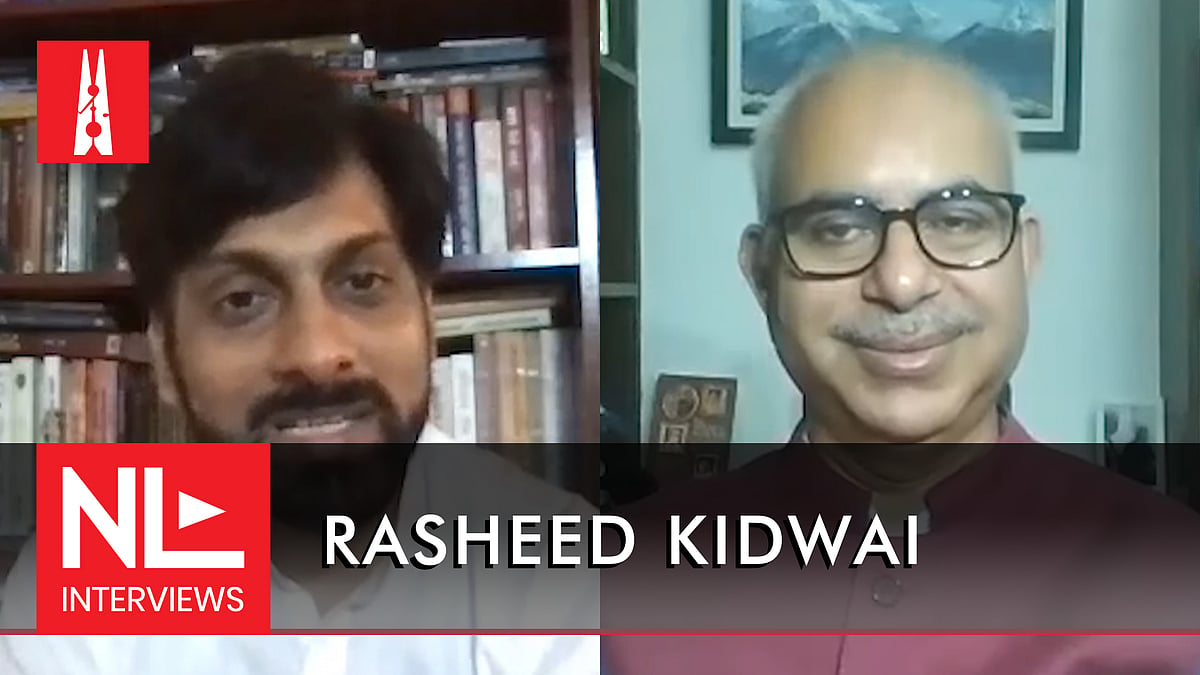 एनएल इंटरव्यू: रशीद किदवई, उनकी किताब 'द हाउस ऑफ़ सिंधियाज़’ और भारतीय राजनीति में सिंधिया घराना
एनएल इंटरव्यू: रशीद किदवई, उनकी किताब 'द हाउस ऑफ़ सिंधियाज़’ और भारतीय राजनीति में सिंधिया घराना