17 सालों का अज्ञातवास: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बुनियादी अधिकारों के अभाव में जीने को मजबूर छत्तीसगढ़ के विस्थापित आदिवासी
ज्यादातर पीने के पानी या बिजली के अभाव में रहते हुए ये लोग, जंगलों से रोजी- रोटी का कोई न कोई जरिया ढूंढ लेते हैं, जहां इनके पास कोई भी जनजातीय अधिकार या जमीन के कागज नहीं हैं.
उस वक्त मडकम संभू की उम्र महज 18 साल थी जब छत्तीसगढ़ के बस्तर में सलवा जुडूम की दहशत भरी हुकूमत की शुरुआत हुई. संभू तब 12वीं कक्षा में पढ़ते थे और चूंकि उनका गांव स्कूल से 15 किमी दूर घने जंगलों के बीच था इसलिए वो बीजापुर में आदिवासी छात्रों के लिए बने एक सरकारी छात्रावस में रहते थे.
वो याद करते हुए बताते हैं, "यह डरावना था. माओवादियों से लड़ने के नाम पर वो लोगों की हत्या कर रहे थें, उन्हें पीट रहे थें, पूरे के पूरे गांव जला रहे थें."
संभू वहां से भाग निकले.
इस सबके 17 सालों बाद संभू न्यूज़लॉन्ड्री को तेलंगाना के मुलुगु जिले के दूरवर्ती स्थान पर स्थित एक छोटे से गांव में मिले. संभू उन हजारों लोगों में से एक हैं जिन्हें सलवा जुडूम ने उनके घरों से उजाड़ दिया. सलवा जुडूम की शुरुआत माओवादियों के दबदबे वाले बस्तर जिले में हुई, यह माओवादियों से लड़ने वाली एक नागरिक सेना थी जिसको राज्य द्वारा समर्थन और सहायता प्राप्त थी. 2005 में बस्तर जिले के कई इलाकों में जुडूम की हुकूमत चलती थी और उन्हें हत्या और बलात्कार समेत पूरे के पूरे गांवों को जला देने जैसी घटनाओं को अंजाम देने की पूरी छूट थी. आज भी कुछ आदिवासी बस्तर के कैंपों में रहते हैं और संभू जैसे बहुत से दूसरे आदिवासी राज्य की सीमाओं को पार कर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहुंच गए.
और वो यहीं रह गए
तेलांगाना में गोदावरी नदी के साथ-साथ मुलुगु, भद्राद्री कोठेगोदेम और खम्मम तक, तो वहीं आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी से लेकर पूर्वी गोदावरी तक ये दोनों राज्य (तेलंगाना और आंध्र प्रदेश) उन 55,000 आदिवासियों का ठिकाना बने हुए हैं जो मूल रूप से छत्तीसगढ़ के हैं. इन लोगों के यहां टिके रहने के बहुत अलग-अलग तरह के कारण हैं. जैसे - गांव-घरों से भगाया जाना, जान बचाकर यहां भाग आना, रोजगार की तलाश आदि. और सन् 2005 से लेकर अब तक इन जिलों के 315 गांवों में कहीं पर भी ये लोग अपने लिए जगह बनाते आ रहे हैं.
घने जंगलों के भीतर या बस्ती और जंगल की सीमाओं के बिल्कुल नजदीक खपरैल की छतों वाली फूस की झोपड़ियों में रहने वाले ये लोग स्थानीय बोली में गुट्टी कोया कहलाते हैं. इनकी ज्यादातर बस्तियों में पानी, बिजली, स्कूल और अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है. अक्सर पूरा का पूरा गांव पीने के पानी के लिए किसी एक बोरवैल या झरने या फिर नदी की एक धारा पर ही आश्रित होता है.
कईयों ने अपनी इस नई जिंदगी के साथ तालमेल बैठा लिया है लेकिन अभी बहुतों को घर लौटने के लिए लंबा इंतजार करना होगा.
यहां भी इन लोगों का अस्तित्व मुश्किलों से अटा पड़ा हुआ है. न्यूज़लॉन्ड्री ने दोनों राज्यों के 30 विस्थापित आदिवासियों से मुलाकात की. इनके नए घरों में जहां इन्हें आदिवासी का दर्जा देने से इंकार कर दिया गया है और "बाहरी" कह कर बुलाया जाता है, साथ ही इनमें हमेशा उजाड़े जाने का डर समाया रहता है. जिस जमीन पर ये लोग खेती करते हैं इनके पास उस जमीन के कागजात भी नहीं है. साथ ही बहुत से लोग माओवादियों या जुडूम की हिंसा से बचकर भागते हुए यहां आये, लेकिन अब ये लोग भागने की सजा भुगतने के डर के साये में जीते हैं.
इसके अलावा इनमें से कुछ लोगों ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर बताया कि इन लोगों और मीडिया व राज्य प्रशासन का रिश्ता काफी अविश्वास भरा है.
एक शख़्स ने कहा, "कृपया मेरी पहचान उजागर मत कीजियेगा. अब भी दोनों तरफ से डर है - पुलिस का भी और माओवादियों का भी."
रोजगार और जान बचाने के लिए प्रवास
प्रवासियों का पहला हुजूम 1950 के दशक के आखिर में उस वक्त आना शुरू हुआ जब छत्तीसगढ़ के आदिवासी मौसमी खेतिहर मजदूरों के तौर पर अविभाजित आंध्र प्रदेश में आना शुरू हुए. वैसे तो इन प्रवासी मजदूरों की संख्या का कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है लेकिन ये लोग हर जनवरी में सीमा को पार करके आंध्र प्रदेश में दाखिल होते थे और चार महीनों तक तंबाकू और मिर्च उगाने का काम करते थे.
दूसरे लोग जमीन की तलाश में यहां आये. उन्हें उम्मीद थी कि वे जो करीब 10 एकड़ जमीन पीछे अपने गांवों में छोड़ आये हैं उसके बदले यहां काफी ज्यादा जमीन हासिल कर लेंगे. जहां इस तरह के लोगों की संख्या का भी कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है वहीं जनजाति कल्याण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि गुट्टी कोया समुदाय की करीब "5-10 प्रतिशत" आबादी ने "आर्थिक कारणों'' से प्रवास के विकल्प को चुना.
भद्राद्री कोठेगुडेम का चिंतलपाड गांव इसी तरह के लोगों की एक शुरुआती बस्ती है. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यह गांव 1990 के दशक के अंत में आबाद होना शुरू हुआ तब यहां छत्तीसगढ़ से आये केवल 12 आदिवासी परिवार ही रहते थे. पोडु पद्धति (जमीन पर उगे पेड़-पौधों को काटकर और जलाकर उसी जमीन पर खेती करने का तरीका) की खेती में लगे ये आदिवासी जंगल के निवासी हैं और खेती करने के इनके इस तरीके की वजह से वन विभाग के अधिकारियों से इनकी टकराव की स्थिति बनी रहती है.



फिर 2005 आया.
छत्तीसगढ़ के सुकमा के सीपीआई (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया) के नेता और पूर्व विधायक मनीष कुंजम का कहना है कि "जुडूम असल में जनता के खिलाफ एक युद्ध था." "सलवा जुडूम के दौर में आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों में से तैनात किये गए विशेष पुलिस अधिकारियों ने दहशत भरी की एक हुकूमत खड़ी कर दी और अनेक लोगों की हत्याएं की. उन्होंने कई गांव जला दिये, जंगल में जो भी इंसान मिला उसको जला डाला, औरतों को प्रताड़ित किया और उनका बलात्कार किया - और कई ऐसे अपराध किये जिनका मैं जिक्र भी नहीं कर सकता."
न्यूज़लॉन्ड्री ने कुंजम से सुकमा में उनके घर के नजदीक ही मुलाकात की. उनका कहना है कि माओवादी अब "पहले से भी ज्यादा ताकतवर" हो चुके हैं और हर गांव में समितियां तैयार कर रहे हैं. साथ ही वे इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि गांव वाले "बिना इजाज़त गांव भी नहीं छोड़ सकते."
उन्होंने भारी मन से माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों के खिलाफ किये गये ऑपरेशन्स की ओर इशारा करते हुए कहा, "माओवादियों ने बहुत से बेगुनाह लोगों की जान ली." "लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा मार आदिवासियों पर पड़ी है. उस दौरान मारे गये बहुत सारे बेगुनाह आदिवासियों का न तो पुलिस से कोई लेना-देना था न ही माओवादियों से."
उन्होंने आगे कहा, "मैं बस उस दौर की यादों को भुला देना चाहता हूं... उस दौर को याद करते हुए आज भी मेरे दिल में दहशत होने लगती है."
संभू भी उन्हीं प्रभावितों में से एक है. उन्होंने बताया कि जुडूम के सदस्यों ने उसके छात्रावास के साथियों से पूछा कि असल में वे किस गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने कहा, "अगर किसी का गांव जुडूम में शामिल न होता तो उसको निशाना बनाया जाता." "वे छात्रों को पीटते थे और उन्हें यातनाएं देते थे."
इस सब से डरे हुए संभू ने अपना सामान बांधा और वहां से अपने गांव के लिए निकल पड़े और खेती-किसानी के काम में अपने परिवार की मदद करने लगे. "मेरी योजना परिस्थितियों में सुधार होने पर छात्रावास में लौटने की थी लेकिन चीजे और भी ज्यादा बिगड़ती चली गयीं."
2006-2007 के बीच संभू के गांव सवनाड को जुडूम द्वारा कई बार "जलाया गया." उन्होंने हमें बताया, "सलवा जुडूम के डर से हम कई-कई दिनों तक जंगलों में ही छिपे रहते थे. वो आते और हम मार डाले जाने के डर से जंगलों में भाग जाते. ऐसे में वो हमारे घरों को जला देते और हमारा सारा अनाज अपने साथ ले जाते."
उन्होंने आगे कहा, "ऐसी परिस्थितियों में कौन यहां रहना चाहता?"
इसलिए उन्होंने एक राहत शिविर का रुख किया जहां उन्होंने 2007 के मध्य तक का समय गुजारा, जब तक कि उन्होंने यह फैसला न कर लिया कि अपने राज्य की सीमा पार करने का वक्त आ गया है.
संभू तीन और लोगों के साथ निकल पड़े और चार दिनों तक पैदल चलकर आज के तेलांगाना में पहुंच गये, अपने सफर में उन्हें कई पहाड़, जंगल और नदियां पार करनी पड़ी.
इस यात्रा में संभू के हमसफर रहे वेट्टाम सतीश ने कहा कि "हम हर रोज 40-50 किमी तक चले." उस वक्त सतीश की उम्र सिर्फ 17 साल थी. "हम तभी सोते जब हमें कोई पानी का स्त्रोत मिल जाता. हम जैसे दूसरे बहुत से लोग थे लेकिन हम में बहुत कम संपर्क होता- हम आज भी नहीं जानते कि कौन कहां गया."
संभू आज से 16 साल पहले अपने इस छोटे से गांव में आकर बस गये. उन्होंने अपना नाम उजागर न करने को कहा है क्योंकि वो आज भी भाग आने के कारण मिलने वाली किसी भी संभावित सजा की आशंका से डरते हैं.


जान बचा कर आंध्र प्रदेश भाग आना
जहां संभू की कहानी जुडूम के डर के इर्द-गिर्द घूमती है वहीं मडकम देवा की कहानी इसके ठीक उलट है.
2005 में देवा की उम्र 20 साल थी. उनका गांव पेड़ाबुरकेल छत्तीसगढ़ के जगरगुंडा के घने जंगलों के बीच स्थित था. गौरतलब है कि उनके गांव में माओवादियों की पकड़ खासी मजबूत थी, और जैसा कि उन्होंने कहा, "वहां पुलिस भी आने की हिम्मत नहीं करती थी."
रोजमर्रा की जिंदगी डर और शंका में डूबी रहती थी. उन्होंने कहा, "दोनों तरफ के लोग, माओवादी और जुडूम एक-दूसरे की जानें ले रहे थे." "अगर आपकी गिरफ़्तारी होती और बाद में आप रिहा कर दिये जाते तो माओवादी यह मानकर आप पर शक करते कि आप ने रिहाई के लिए किसी तरह के समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं. और अगर माओवादी घर आ जाते तो जुडूम आपको खबरी समझकर, निशाना बनाता."
उन्होंने आगे कहा, "तो इस तरह हम आदिवासी माओवादियों और जूडुम की लड़ाई में हमेशा मार झेलने वाली तरफ ही रहते."
देवा जो अब 35 साल के हैं, ने हमें बताया कि 2007 की शुरुआत में सलवा जुडूम के सदस्यों ने उनके गांव वालों को बताया कि वे खतरे में है. "उन्होंने हमें बताया कि सरकार ने माओवादियों को मारने का आदेश दिया है और अगर हम जुडूम में शामिल नहीं होंगे तो क्रॉस-फायरिंग में हम भी मार डाले जायेंगे." "इसलिए हम जुडूम के कैंपों में आकर रहने लगे."
देवा करते हैं कि कैंपों में किस तरह गांव वालों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी.
"लेकिन हमें यह पसंद नहीं आया इसलिए हमने इंकार कर दिया", उन्होंने जल्दी से अपनी बात में जोड़ा. "दूसरे कामों में पड़ोस के गांवों पर नजर रखना शामिल था ताकि नक्सलियों की गतिविधियों को ट्रैक किया जा सके. लेकिन नक्सली भी जाल बिछाकर रखते और जुडूम के लोगों से मुठभेड़ करते. दोनों तरफ के लोग एक-दूसरे को मार रहे थे. कुछ भी निश्चित नहीं था और कभी भी, कहीं भी, किसी की भी जान जा सकती थी."
कैंप की जिंदगी कुछ दूसरे कारणों से भी उनके अनुकूल नहीं थी. उन्होंने कहा, "हम आदिवासियों का कैंप में क्या काम? हमारा रिश्ता तो जंगलों से है."
इसलिए देवा ने कैंप छोड़ने का फैसला लिया. उनके भाई जो कैंप में उनके साथ थे, पहले ही जा चुके थे, और तेलंगाना के मलुंगुर की ओर बढ़ रहे थे. इसलिए देवा ने सोचा कि उनके जाने का वक्त भी आ चुका है. उन्होंने बताया, "मैं कुछ सुरक्षा कर्मियों के साथ पैदल दंतेवाड़ा के पलनाड गया. "वहां से मैंने भद्राचलम के लिए बस ली." और भद्राचलम, जो कि तेलंगाना में गोदावरी नदी के किनारे बसा एक कस्बा है, से मलुंगुर की ओर चल पड़ा.
लेकिन देवा की परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई. कुछ दिनों बाद पेड़ाबुरकेल से दो गांव वाले आ धमके और उनसे कहा कि वो उन्हें "वापस ले जाने आये हैं." देवा ने न्यूज़लॉन्ड्री से कहा, "उन्होंने कहा कि मुझे वापस गांव लौट आना चाहिए और वहीं शांति से जिंदगी गुजारनी चाहिए."
गांव में वापस लौटने पर उन्हें एक ग्राम स्तर की माओवादी समिति ने, वह आंध्र प्रदेश "भागकर क्यों गए" और जुडूम के कैंप में वो क्या कर रहे थे, जैसे सवालों के जरिये "परेशान" किया. समिति उनके जवाबों से संतुष्ट तो लगी लेकिन उसने इस पर जोर दिया कि उन्हें पेड़ाबुरकेल में ही रहना होगा.
देवा इस सब से परेशान थे. उन्होंने कहा, "ऐसी अफवाहें थीं कि मुझे खत्म कर दिया जाएगा." और हजारों ऐसे आदिवासियों का यही हाल हुआ था, जिन पर "खबरी" होने का शक था. इसलिए उन्होंने दोबारा अपना सामान बांध लिया.
उन्होंने याद करते हुए कहा, "मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा, जिंदा रहेगा तो कहीं पर भी जी लेगा, यहां तेरा खतरा है."
ये शब्द उन्हें खौफ से भर देते थे. इसलिए 24 मई, 2007 की सुबह पेड़ाबुरकेल से भाग निकले. देवा आठ घंटे तक लगातार, बिना रुके अपनी साइकिल चलाते रहे. जब तक कि वह आंध्र प्रदेश की सीमा पर नहीं पहुंच गये. उन्होंने भद्राचलम के लिए एक बस ली और फिर एक बस मलुंगुर के लिए ली.
उन्होंने कहा, "और बस. तब से, मैं फिर कभी घर लौटकर नहीं गया."
2008 तक उनके परिवार के कुछ सदस्य उनके साथ तेलंगाना में आकर रहने लगे. अब ये परिवार भद्राचलम के नजदीक कृष्णासागर ग्राम पंचायत के देवायागूम गांव में रहता है, जहां देवा अब एक किसान के तौर पर जिंदगी गुजारते हैं.
'अतिक्रमण' और वनीकरण
तेलंगाना के खम्मम जिले में डॉ० एसके हनीफ सितारा एसोसिएशन नाम का एनजीओ चलाते हैं. यह एनजीओ स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और आदिवासियों के अधिकारों के लिए काम करता है. उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ से आये आदिवासियों और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आदिवासियों के बीच समानताएं हैं- दोनों ही विशाल कोया जनजाति से संबंधित हैं.
उन्होंने इसे समझाते हुए कहा, "इसलिए जब हजारों आदिवासी 2005 के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भागकर आये तो स्थानीय कोया लोगों ने उन्हें यहां बसने में मदद की और जंगलों को काटने और खेतिहर मजदूरों के तौर पर सस्ते श्रम के लिए इनका इस्तेमाल किया. समय बीतने पर इन विस्थापित आदिवासियों ने जंगलों की जमीन पर अपने गांव स्थापित किये और खुद की खेती के लिए जंगलों को काटना शुरू किया.
जहां 2005 से पहले दोनों राज्यों में कुल मिलाकर करीब 35 गुट्टी कोया परिवार थें वहीं 2005 के बाद ऐसे गांवों की संख्या बढ़कर 315 हो गयी क्योंकि अब सलवा जुडूम के डर से आदिवासी भागकर यहां आने लगे थे. जनजाति मामलों के वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा, "करीब 90 प्रतिशत" गुट्टी कोया आदिवासी 2005 के बाद यहां आये हैं.
उदाहरण के लिए चिंतलपाड़ गांव को ही ले लीजिए, इस शुरुआती बस्ती के बारे में पहले ही बताया गया था कि 1990 के दशक तक यहां केवल 12 गुट्टी कोया परिवार रहते थें लेकिन गांव के प्रधान मरियम सुनील के मुताबिक अब यहां करीब 60 ऐसे परिवारों का घर है."


लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां रहने वाला हर परिवार जुडूम के डर से भाग कर आया है. 2005 से यहां रहने वाले ग्रामीण कट्टम कोसा का कहना है कि "हमारे गांव में बहुत से लोग रहने के लिए आये." "जिनमें से ज्यादातर बाद में आस-पास के इलाकों में अलग बस्तियां बनाने के लिए यहां से चले गये."
गुट्टी कोया ज्यादातर खेती की पोडु पद्धति में लगे हुए हैं जिस वजह से वे अपने आप ही वन-अधिकारियों के खिलाफ खड़े दिखाई देने लगते हैं. नाम न उजागर करने की शर्त पर भद्राद्री कोठुगोदेम के एक वन अधिकारी ने कहा, "असल परेशानी इन लोगों का तेजी से होता विस्तार है, जो जंगल की जमीन का अतिक्रमण कर रहा है." "गुट्टी कोया की तरह कोई भी दूसरी स्थानीय जनजाति जंगलों में नहीं रहती. हम किसी को भी इतने ज्यादा घने जंगलों के बीच घर बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते."
तेलंगाना वन विभाग के अनुसार भद्राद्री कोठुगुडेम की तीन लाख एकड़ वन भूमि पर 'अतिक्रमण करने वालों' का कब्जा हो चुका है. अधिकारी ने यह भी कहा कि "अगर इसी दर से अतिक्रमण जारी रहा तो 10 साल बाद जिले में बिल्कुल भी वन्य भूमि नहीं बचेगी."
हालांकि इसमें से सिर्फ 10 प्रतिशत जमीन ही गुट्टी कोया समुदाय के लोगों द्वारा अतिक्रमित की गयी है. बाकी की जमीन पर स्थानीय लोगों का ही कब्जा है. फिर भी इस आक्रोश की पहली पंक्ति में वे विस्थापित आदिवासी ही हैं जिनमें से किसी के पास भी इन जमीनों के कागजात नहीं है.
इनमें से कुछ लोगों ने न्यूज़लॉन्ड्री को बताया कि उनको इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि स्थानीय लोग भी ठीक इसी तरह अतिक्रमण करते हैं, जैसा कि एक आदिवासी ने कहा "और उन्हें स्थानीय होने के कारण ये काम करने में आसानी होती है.” उसने आगे कहा, "लेकिन अगर हम इस पर कुछ कहेंगे तो हमें बाहरी करार दे दिया जायेगा और वन अधिकारियों का उत्पीड़न झेलना पड़ेगा."
राज्य में वृक्ष आच्छादित जमीन का प्रतिशत 24 से बढ़ाकर 33 करने के लिए तेलंगाना वन विभाग द्वारा अपने बैनर तले हरिता हरम नामक वनीकरण अभियान चला रहा है. हालांकि इस अभियान की वजह से बहुत से गुट्टी कोया भूमिहीन हो गये है. तो कुछ ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा खो दिया है, कई अन्य का दावा है कि उन्होंने करीब 100 एकड़ जमीन खो दी है क्योंकि वन कर्मियों ने उनकी खेती की जमीन वृक्षारोपण के लिए ले ली है.
विस्थापित आदिवासियों ने न्यूज़लॉन्ड्री को बताया कि वे अपनी खेती छोड़कर खेतों में और चावल के मिलों में दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं. तेलंगाना के मुलुगु में रहने वाले इनमें से एक आदिवासी ने कहा, "हमें जंगलों से बाहर निकालने के लिए वन विभाग पहले हमारी झोपड़ियों को गिरा या जला देता था लेकिन अब उन्होंने वृक्षारोपण के लिए हमारी जमीनें लेनी शुरू कर दी है."
कुछ आदिवासियों द्वारा दायर की गयी याचिका के आधार पर 2018 में यह मामला तेलंगाना हाईकोर्ट में पहुंच गया. जहां एक ओर अदालत ने प्रशासन को "झोपड़ियों, रहने की जगहों और दूसरे ढांचों को तोड़ने से" रोक दिया वहीं उसने गुट्टी कोया से भी यह कहा कि उनकी खेती के काम में "किसी पेड़ को काटकर गिराना या जमीन की भौतिक स्थिति में किसी तरह की कोई कांट-छांट शामिल नहीं होनी चाहिए."
संभू के साथ छत्तीसगढ़ के अपने गांव से भागने वाले सतीश पर एक आरोप है कि "वनीकरण" की वजह से उन्होंने अपनी "करीब 10 एकड़ जमीन" खो दी.
सतीश मूल रूप से छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कोचोली गांव से हैं. 2005 में जब सलवा जुडूम की दहशत के दिन शुरू हुए तो उस वक्त वो स्कूल में पढ़ते थे. सतीश ने कहा, "ये बात हर तरफ फैल गयी कि जो लोग भी पढ़ रहे हैं उन्हें पुलिस की नौकरी मिल जायेगी. माओवादियों ने इसे एक समस्या की तरह देखा." "उन्होंने हमारे हाथों को पीछे बांधकर हमें बेरहमी से पीटा. पुलिस ने भी यह कहकर हमें ही निशाना बनाया कि हम माओवादी बन जाएंगे. हमारी जिंदगी नर्क बन गयी थी."
सतीश ने संभू और दो अन्य लोगों के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा पर कर ली. उन्होंने आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद पर अपनी नजर जमा रखी थी और 2006 में उस शहर को अपना घर बना लिया. हैदराबाद में सतीश एक मजदूर के तौर पर काम करते थे जबकि उनके भाई छत्तीसगढ़ के उनके गांव में ही थे.
तीन साल बाद उनको कहीं से यह बात पता लगी कि उनके अपने गांव के कुछ लोग मुलुगु के मोतलागुडम में आकर बस गए हैं.
सतीश ने कहा, "खेती अब भी मेरी पहली प्राथमिकता नहीं थी. मैं चेरला (तेलंगाना) में एक दुकान जमाने की योजना बना रहा था." "लेकिन तभी मुझे गांव के कुछ लोगों से सुनने को मिला कि यह कोई अच्छी तरकीब नहीं है क्योंकि इससे मैं माओवादियों के निशाने पर आ जाऊंगा."
क्यों निशाने पर आ जाएंगे? "मेरे मोबाइल की वजह से!" उन्होंने कहा. उस वक्त मेरे पास एक मोबाइल फोन था. उन्होंने मुझे उस पर बात करते देख लिया था. इसकी वजह से वो यह सोचने लगे कि मैं इसका इस्तेमाल पुलिस को उनकी गतिविधियों के बारे में बताने के लिए करने लगूंगा."
सतीश ने अपनी योजना बीच में ही छोड़ दी और अपने गांव वालों के साथ मुलुगु जिले के मोटलागुडम जिले में खेती के लिए जंगलों की कटाई का काम करने लगे. उन्होंने बताया कि उन्हें खेती के लिए 10 एकड़ की जमीन को साफ करने में तीन साल लग गये. और इसके आठ साल बाद ये जमीन वन विभाग ने अपने कब्जे में ले ली.
हताश हो चुके सतीश ने कहा, "पूरे एक साल के लिए, मैं हर सुबह जल्दी उठता, काम पर जाता और रात को ही वापस लौटकर आता." "मैंने एक झटके में सब खो दिया." सतीश के पास अब सिर्फ आधा एकड़ जमीन है लेकिन उस पर खेती करने के लिए उनके मन में कोई उत्साह नहीं है. "अब मैं इसका क्या करूंगा?" उन्होंने सवाल किया.
लेकिन भद्राद्री के एक वन अधिकारी का कहना है कि वनीकरण अभियान "बेहद शांतिपूर्ण" रहा और विभाग ने 2015 से लेकर अब तक कुल 45000 एकड़ जमीन "वापस बरामद" कर ली है. अधिकारी ने कहा, "हम उन्हें यह समझाने में सफल रहें कि 'थोड़ा हमें दो और थोड़ा अपने लिए रखो," "और ये तरीका बहुत कारगर रहा."
न जमीन मिली, न ही आदिवासी का दर्जा
विस्थापित आदिवासी मोटे तौर पर दो अनसुलझी समस्याओं से जूझ रहे हैं. पहली उनकी जमीन से जुड़ी है और दूसरी उन्हें आदिवासी का दर्जा मिलने से.
नवंबर में तेलंगाना सरकार ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत आदिवासियों को जमीन दिलाने के लिए एक सर्वे की शुरुआत की. यह अधिनियम आदिवासियों और "पारंपरिक तौर पर जंगलों में रहने वालों" को जंगल की जमीन के अधिकार देता है बशर्ते वो इन इलाकों में 13 दिसंबर, 2005 से पहले से रह रहे हो.
यह सर्वे राज्य के 28 जिलों के 37 मंडलों के 3,041 गांवों में किया गया जिसमें गुट्टी कोया बस्तियां भी शामिल थी. और बहुत से गुट्टी कोया अपनी जमीन के लिए पट्टा, या कागज मिलने की उम्मीद कर रहे थे
लेकिन 22 नवंबर को भद्राद्री कोठेगुडम जिले के बेंडालापाडु में एर्राबोडु नामक गुट्टी कोयाओं की छोटी-सी बस्ती में एक वन अधिकारी की हत्या हो गयी. यह हत्या उस इलाके को गुट्टी कोया आदिवासियों से खाली कराने के दौरान हुई. वन विभाग द्वारा यह कार्रवाई इसलिए की जा रही थी क्योंकि कथित तौर पर गुट्टी कोया समुदाय के लोग जंगल की जमीन पर मवेशी चराते थे. इस हत्या के बाद वन कर्मी विरोध प्रदर्शन करने लगे और न्याय के नाम पर गुट्टी कोयाओं को वहां से भगाये जाने की मांग करने लगे.


26 नवंबर को वहां की स्थानीय ग्राम पंचायत ने भी एक प्रस्ताव पास कर एर्राबोडु में हुई हत्या की वजह से गुट्टी कोयाओं को समाज से बाहर कर दिया, और यहां तक कह दिया कि इस समुदाय के सभी लोगों को वापस छत्तीसगढ़ भेज दिया जाए. तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देते हुए इस प्रस्ताव को 5 दिसंबर को खारिज कर दिया.
लेकिन पहले से ही विस्थापित आदिवासियों का जो भी नुकसान होना था, हो चुका था. देवा ने कहा, "पहले जब अधिकारी सर्वे कर के गये तब मुझे अपनी जमीन के लिए पट्टा मिलने की उम्मीद थी." "लेकिन हत्या ने सारी उम्मीदें खत्म कर दी."
चिंतलपाड के मडकम सुनील ने कहा, "अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो क्या इसका ये मतलब है कि पूरा समुदाय ही गुनहगार है? हम सब इस हत्या की निंदा करते हैं. गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए, पर क्या ये ठीक है कि एक आदमी की गलती के लिए पूरे समुदाय को इसकी सजा दी जाये?"
हालांकि तेलंगाना सरकार के जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हत्या और सर्वे दो अलग-अलग मामले हैं इसलिए भूमि अधिकारों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.
अब ये हमें दूसरे मुद्दे पर ले आता है - आदिवासी का दर्जा मिलने पर.
एक अधिकारी ने न्यूज़लॉन्ड्री को बताया कि "किसी भी गुट्टी कोया को जमीन के हक नहीं मिलेंगे. उन्हें तेलंगाना में आदिवासी नहीं माना जाता. कृपया इस बात को समझिए कि भूमि अधिकार अधिनियम उन आदिवासियों के लिए है, जिनकी ऐतिहासिक तौर पर अनदेखी की गयी है."
छत्तीसगढ़ में विस्थापित आदिवासियों को अनूसूचित जनजाति माना जाता है. लेकिन गुट्टी कोयाओं को छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में अनूसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला है - शायद इसलिए क्योंकि उनके समुदाय का नाम आधिकारिक नहीं है, और ये एक स्थानीय नाम है.
कुंजम का कहना है कि "हम इस गुट्टी कोया नाम से ठीक तरह से वाकिफ नहीं है. यह एक स्थानीय नाम है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रहने वाले हमारे लोगों को दे दिया गया है. हमारे राजस्व के रिकॉर्ड्स में हमें मुरिया या मारिया और कुछ मामलों में तो, गोंड नाम भी दे दिया गया है."
गौरतलब है कि मुरिया या मोरिया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक अधिसूचित जनजाति है जिसकी वजह से इन्हें इन दोनों ही राज्यों में अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिल पा रहा है, उन्होंने समझाया.
उन्होंने आगे जोड़ा "वे लोग इस वजह से वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) के तहत लाभ नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि एफआरए के नियम स्पष्ट तौर पर यह कहते हैं कि गैर आदिवासी मामले में उक्त व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि दिसंबर 2005 से कम से कम 75 साल पहले से उसका संबंधित जमीन के टुकड़े पर कब्जा था, और 75 साल पुराने कागजात पेश करना इन लोगों के लिए मुमकिन नहीं है."
स्थानीय कोया नेता और राज्य में आदिवासी कर्मचारी यूनियन के कार्यकारी सदस्य बुग्गा रामानाधम का कहना है कि यह ठीक नहीं है.
उनका कहना है कि "गुट्टी कोया का संबंध उसी कोया जनजाति से है जिसके नाम से तेलंगाना की स्थानीय जनजाति को जाना जाता है." "इन्हें छत्तीसगढ़ में एक जनजाति माना जाता है. अधिकारियों द्वारा उनको गुट्टी कोया बुलाया जाना एक गलत समझ का नतीजा है. राज्यों की सीमाएं सरकारों द्वारा तय की जाती है न कि जनजातियों द्वारा."
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोगों की पहचान व जगहों के नाम बदल दिये गए हैं.
तीन भागों में आने वाली रिपोर्ट्स की श्रृंखला का यह पहला भाग है.
न्यूज़लॉन्ड्री की यह रिपोर्ट पहले अंग्रेज़ी में प्रकाशित हुई थी जिसे आप यहां पढ़ सकते हैं.
 दरकता जोशीमठ: करीब 700 मकानों में दरारें, घरों को कराया जा रहा खाली
दरकता जोशीमठ: करीब 700 मकानों में दरारें, घरों को कराया जा रहा खाली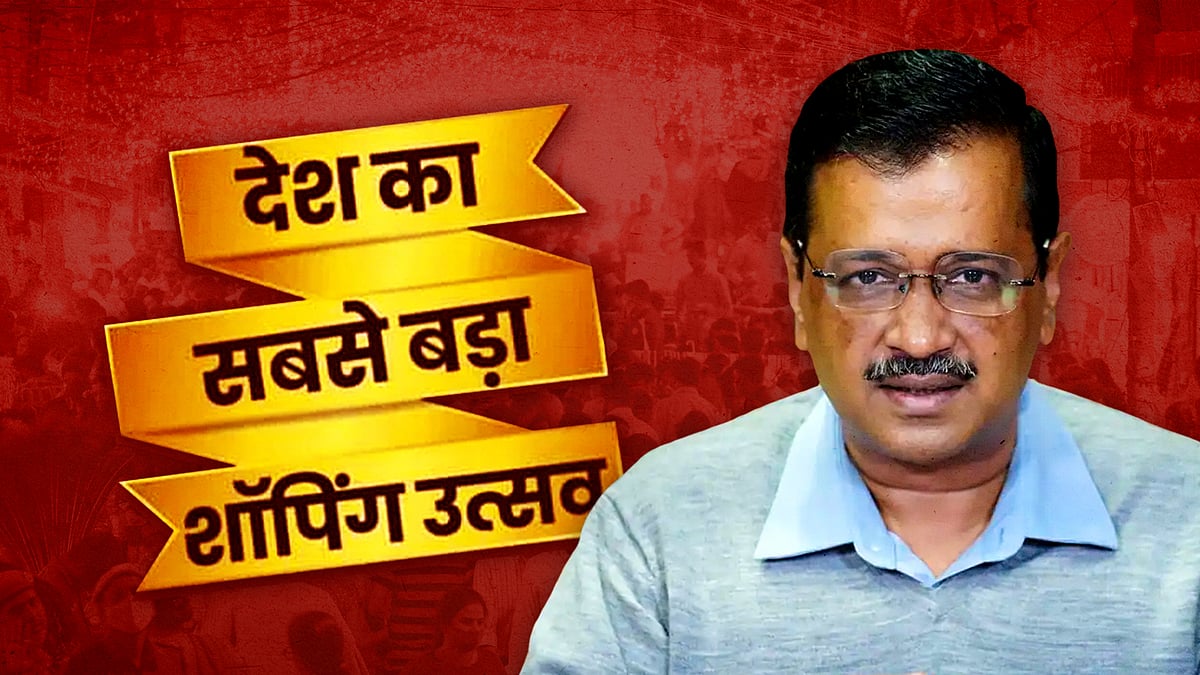 दिल्ली सरकार का बहुप्रचारित ‘दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल’ 28 जनवरी से नहीं होगा, पर क्यों?
दिल्ली सरकार का बहुप्रचारित ‘दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल’ 28 जनवरी से नहीं होगा, पर क्यों?